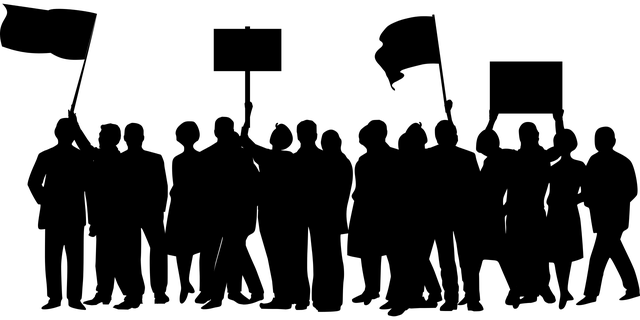by
बी.एस. चैहान ‘चेत’ पी. ओ. चिऊणी, तह. थुनाग, जिला मण्डी-175048 टी.जी.टी. कला रा.वमा. पाठशाला, छाट (छलवाटन)
Contact: 94184-03136 email: [email protected]
हिमाचल प्रदेश बनने से पूर्व कई प्रसिद्ध जन–आन्दोलन हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आजादी की चिंगारी धीरे–धीरे फैलती रही। बहुत लम्बे समय से यहां की जनता स्थानीय शासकों की निरंकुशता, शोषण, हिंसा और अन्याय सहती रही। काफी जुल्म सहने के बाद भोली–भाली जनता का आक्रोश फूट पड़ा है और जनता ने शासकों के विरूद्ध आन्दोलन करने शुरू कर दिए। हर इन्सान या जीव स्वतंत्र रहना चाहता है। यह अधीनता चाहे स्थानीय निरंकुश शासकों से हो या फिर विदेशी आक्रान्ताओं से। हिमाचल के पहाड़ी लोगों ने सदा ही बाहरी आक्रमकों तथा भीतरी दमन का विरोध किया है।
हिमाचल प्रदेश में ये जन–आन्दोलन तीन प्रकार से चले। एक वो जो किसी विशेष स्थान के लोगों ने अपनी स्थानीय समस्याओं को लेकर चलाये। ये अधिकांश भूमि, भूमि बन्दोबस्त, भूमि लगान , बेठ–बेगार, राजा या उसके कर्मचारियों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ होते थे। 9 मार्च 1846 की सन्धि के अनुसार वर्तमान हिमाचल के अधिकांश हिस्से सिक्खों से छूटकर सीधे अंग्र्रेजी प्रशासन के अधीन आ गए, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेजों का एकाधीकार स्थापित हो गया। अब पहाड़ी रियासतों के राजा आपस में नहीं लड़ सकते थे। क्योंकि सभी शासक अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों को सिर्फ बेगार और कर राशि से मतलब था। नूरपुर के राजा जसवंत सिंह को अंग्रेजों ने 5000 रु. वार्षिक देकर अपने कब्जे में ले लिया।
सन् 1848 ई. का दूसरा अंग्रेज सिक्ख युद्ध आरम्भ हुआ उसी समय “राम सिंह” ने आक्रमण करके अंग्रेजी सेना को भगा दिया और वहां पर नूरपुर का झण्डा लहरा दिया। राम सिंह को बाद में विपरित परिस्थितियों के कारण मैदान छोड़ कर भागना पड़ा। जब वह पहाड़ों पर वापिस आया तो उसके एक मित्र द्र्रोही पहाड़ चन्द ने अंग्रेजों के हाथों उसे पकड़वा दिया। अंग्रेजों ने राम सिंह को काले पानी की सजा देकर उसे सिंगापुर भेज दिया। नूरपुर रियासत के इतिहास में वजीर राम सिंह का महत्त्वपूर्ण योगदान है।
1857 के विद्रोह का प्रभाव हिमाचल की पहाड़ी रियासतों पर भी पड़ा। यहां पर जहां एक ओर देशभक्तों ने अंग्रजों के विरूद्ध आवाज उठाई तो वहीं दूसरी ओर अनेक राजाओं ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ भी दिया। 1857 ई. के विद्रोह के परिणामस्वरूप रामपुर के राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजी सता के विरूद्ध आवाज उठाई। उस समय उस सेना में अधिकांश सैनिक गोरखा और राजपूत थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु संघर्ष तेज करने के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर प्रजामण्डलों की स्थापना की गई। स्वतन्त्रता पूर्व बुशहर, शिमला हिल स्टेटस में शामिल था। 1939 ई. में लुधियाना
में “All India State Peoples” हुई, जिसमें “The Himachal Riyasti Praja Mandal” की स्थापना की गई। बुशहर में प. पदम देव ने प्रजामण्डल का नेतृत्व किया।
हिमाचल प्रदेश के जन–आन्दोलन इस प्रकार है।
1. सुकेत जन–आन्दोलन (1862-1876)- सुकेत के राजा उग्रसेन का वजीर नरोत्तम एक अत्याचारी प्रशासक था। जनता उससे बहुत दुःखी थी। उसने कुछ ब्राह्मण परिवारों पर दण्ड लगाया था। लोगांे ने इसका विरोध किया और गिरफ्तार करने की मांग की। राजा के पुत्र रूद्र सेन ने भी उस वजीर का विरोध किया। अन्त में राजा ने वजीर नरोत्तम को हटा दिया और उसके स्थान पर ‘धुंगल’ को वजीर बनाया।
2. नालागढ़ जन–आन्दोलन (1877)- नालागढ़ के हिंडूर की राजगद्दी पर राजा ईश्वरी सिंह 1877 ई. में बैठा था। उसके समय में राजा का वजीर गुलाम कादिर खान था। इसने प्रजा पर नए कर लगा दिए और भूमि लगान बढ़ा दिए। इसका नालागढ़ की प्रजा ने विद्रोह किया। अन्त में राजा को जनता की मांगों को मानने के लिए विवश होना पड़ा और वजीर कादिर खान को निकाल दिया गया।
3. सुकेत जन–आन्दोलन (1878)- सुकेत का जन–आन्दोलन 1878 ई. में हुआ। 1876 ई. में रूद्रसेन गद्दी पर बैठा, फिर उसने ‘धुंगल’ को वजीर बनाया था, उसने किसानों और जमींदारों पर नए कर लगा दिए। किसानों पर –चार रु’ ‘आठ रु’ प्रति खार लगभग 8 क्विंटल कर लगाया। इस कर को वजीर ‘धुंगल’ ने‘ ‘ढाल’ नाम दिया। लोगों ने राजा से न्याय की मांग की परन्तु राजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया इस पर लोगों ने आन्दोलन करने शुरू कर दिए और अन्त में राजा को भी गद्दी से हटा दिया गया। सारे कर हटा दिए।
4. चम्बा का किसान आन्दोलन (1895)- चम्बा का किसान आन्दोलन 1895 में हुआ। उस समय चम्बा रियासत का राजा शाम सिंह था। राजा शाम सिंह और उसके वजीर गोविन्द राम के प्रशासन में किसानों पर भूमि–लगान का भारी बोझ था। इसके अतिरिक्त बेगार भी अधिक ली जाने लगी। अतः लोगों ने राजा से लगान कम करने और बेगार बंद करने के लिए अनुरोध किया, परन्तु राजा ने कोई परवाह न की। यह देखकर चम्बा के भटियात क्षेत्र के किसानों ने इसके विरूद्ध आन्दोलन आरम्भ कर दिया। रियासत की सरकार ने इसे विद्रोह का नाम देकर दबाने का प्रयास किया परन्तु वह असफल रही। फिर अंग्रेज सरकार ने हस्तक्षेप करके इसे दृढ़ता से दबा दिया।
5. बाघल में भूमि आन्दोलन (1897)- बाघल में 1897 ई. में रियासत के राजा ध्यान सिंह के समय में अत्यधिक भूमि लगान के विरोध में 1902 तक लोगों ने आन्दोलन चलाया। भूमि लगान में भारी वृद्धि, चारागाहों की कमी तथा उन जंगली जानवरों के मारने पर रोक लगाने, जो किसानों की फसलों को नष्ट कर देते थे, के विरोध में किसानों ने आन्दोलन किए।
6. क्योंथल में भूमि आन्दोलन (1897)- 1897 ई. में क्योंथल रियासत में भी भूमि आन्दोलन हुआ। चार परगना के लोगों ने लगान और बेगार देना बन्द कर दिया। अंग्रेज अधिकारी सैडमैन और टामस ने इस असंतोष को समाप्त कराने के लिए राजा बलवीर सेन से कहा परन्तु वह असफल रहा। अतः में अंग्रेज सरकार ने मियां दुर्गा सिंह को बतौर मैनेजर बनाकर 11 जुलाई 1898 को नियुक्त किया जिसने इस आन्दोलन पर काबू पा लिया।
7. ठियोग और बेजा में आन्दोलन (1878)- बेजा और ठियोग ठकुराइयों में भी 1898 में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। बेजा की जनता ने ठाकुर के विरूद्ध आन्दोलन किया तथा रियासत के दो सिपाही भी बंदी बना दिए। बेजा के शासक उदय चंद ने अंग्रेजों की सहायता से इस आन्दोलन को दबा दिया। ठियोग ठकुराई में बंदोबस्त में गड़बड़ी के विरोध मंे 1898 में ही किसानों द्वारा आन्दोलन चलाया गया, और किसानों ने बेगार देने से इंकार कर दिया। रियासती सरकार ने अंग्रेज सरकार की सहायता से लोगों को शांत किया गया।
8. बाघल में विद्रोह (1905)- बाघल रियासत में 1905 में पुनः विद्रोह हुआ। उस समय बाघल रियासत का राजा विक्रम सिंह था जो उस समय अवयस्क था। इसलिए राज्य का प्रबन्ध मियां मान सिंह के हाथ में था। इस विद्रोह का आरम्भ राज परिवार के आंतरिक षडयंत्र से हुआ।
9. डोडरा क्वार में विद्रोह (1906)- 1906 ई. में बुशैहर के गढ़वाल के साथ लगते क्षेत्र डोडरा क्वार में एक विद्रोह हुआ। इस क्षेत्र का प्रशासन राजा की ओर से किन्नौर के गांव ‘पवारी’ के वंशनुगत वजीर परिवार के ‘रणबहादुर सिंह’ के हाथ में था। उसने राजा के विरूद्ध विद्रोह करके डोडरा–क्वार को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया। वहां की जनता ने भी उसका साथ दिया था। परन्तु बाद में रणबहादुर सिंह को कैद कर लिया और उसे मुक्त भी किया गया परन्तु शिमला में उसकी मृत्यु हो गई।
10. मण्डी में किसान आन्दोलन (1909)- मंडी में राजा भवानी सेन के समय में 1909 में किसानों द्वारा आन्दोलन किया गया। राजा के वजीर ‘जीवानंद पाधा’ के अत्याचार और उसके द्वारा रियासत में फैलाए गए भ्रष्टाचार तथा आर्थिक शोषण से वहां की जनता परेशान थी। ऐसी स्थिति में सरकाघाट क्षेत्र से शोभाराम 20 व्यक्तियों का एक शिष्ट मण्डल अपनी शिकायतों को लेकर राजा के पास मण्डी आया। राजा ने वजीर की बातों में आकर शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दिया। अन्त में राजा भवानी सेन को अंगे्रजी सरकार से मदद लेनी पड़ी। बाद में जनता की मांग पर वजीर जीवानंद को पदच्युत कर दिया गया और राजेन्द्र पाल को राजा का सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद मण्डी के किसानों के करों में कमी की गई और जनता की मांग पूरी होने के बाद आन्दोलन समाप्त हो गया।
11. सुकेत में जन–आन्दोलन (1924-26)- सुकेत में 1878 ई. के बाद 1924-26 में भी एक जन–आन्दोलन हुआ था। सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन के काल में जनता से जरूरत से अधिक लगान लिया जाता था। बेगार प्रथा भी जोरों पर थी। राजा के नाम से ‘लक्ष्मण’ कानून चलाया जाता था। 1924 में जब बेगार, लगान और करों से जनता परेशान हो गई, तब जनता ने आन्दोलन शुरू किया। इस आन्दोलन का नेतृत्व सुन्दरनगर (वनैड) के मियां रत्न सिंह ने किया। लोगों ने मियां रत्न सिंह के नेतृत्व में कचहरी का घेराव किया। स्थिति को नाजुक देखकर रत्न सिंह ने लोगों को शान्त रहने का कहा। मियां रत्न सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों को डरा कर यहां–वहां कर दिया। 42 व्यक्ति पकड़े गए और उन्हें जालन्धर, रावलपिंडी आदि जेलों में रखा गया।
12. सिरमौर में आन्दोलन (1929)- 1929 में भूमि बन्दोबस्त के विरोध में सिरमौर मेें पांवटा साहिब और नाहन में लोगों ने पं. राजेन्द्र दत्त के नेतृत्व में आन्दोलन किया। राजा अमर प्रकाश और अंग्रेज सरकार को पांवटा के लोगों ने संदेश भेजे। राज्य सरकार के कहने पर आन्दोलन को दबाने का प्रयास किया और थोड़े समय के बाद सिरमौर में जन–आन्दोलन शान्ति से समाप्त हो गया।
13. बिलासपुर में जन–आन्दोलन (1930)- बिलासपुर में 1930 मेें भूमि बन्दोबस्त के कारण जन–आन्दोलन हुआ। सबसे पहले परगना बहादुरपुर के लोगों ने बन्दोबस्त के विरूद्ध आन्दोलन शुरू हुआ। उन्होंने बन्दोबस्त के कर्मचारियों को लकड़ी, दूध, घी, रोटी आदि मुफ्त देना बन्द कर दिया। बहादुरपुर के लोगों ने तंग आकर पटवारियों के पैमाईश के सामान को तोड–फोड़ दिया। पुलिस नमहोल गांव मेें मेले के अवसर पर एकत्रित कुछ आन्दोलनकारियों को पकड़कर बिलासपुर ले गई। कुछ आन्दोलनकारियों को हिरासत में लेकर जेलों में बन्द कर दिया। पुलिस द्वारा इस बगावत में डण्डा चलाने के कारण इस आन्दोलन का नाम ‘डाण्डरा’ आन्दोलन पड़ गया।
14. सिरमौर का पझौता किसान आन्दोलन (1942-43)- जब सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र पझौता में किसान आन्दोलन शुरू हुआ उन दिनों दूसरा विश्वयुद्ध जोरों पर था। बंगाल मेें भारी अकाल पड़ा था। अनाज की कमी हो रही थी। इसलिये रियासती सरकार ने किसानों पर रियासत से बाहर अनाज भेजने पर रोक लगा दी जहां बेचने पर अच्छे मूल्य मिलते थे। किसानों को यह भी आदेश दिया गया कि वे लोग अपने पास थोड़ा अन्न रखे शेष अन्न सरकारी को–आपरेटिसव सोसायटियों मंे बेच दें। पझौता के गांव टपरौली में अक्तूबर 1942 को किसान एकत्रित हुए और स्थिति से निपटने के लिए ‘पझौता किसान सभा’ का गठन किया। इस सभा के प्रधान ‘लक्ष्मी सिंह’ गांव कोटला तथा सचिव वैद्य सूरत सिंह कटोगड़ा चुने गये। इनके अलावा इस सभा में मियां–चूं–चूं, मियां गुलाब सिंह आदि शामिल थे। इस आन्दोलन का समूचा नियंत्रण व सचांलन वैद्य सूरत सिंह के हाथ में था। उसने राजा राजेन्द्र प्रकाश को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह स्वयं लोगों की परेशनियां जानने के लिए इलाके का दौरा करें। परन्तु राजा अपने कर्मचारियों की चापलूसी पर आश्रित था। कर्मचारियों ने राजा को लोगों से मिलने नहीं दिया।